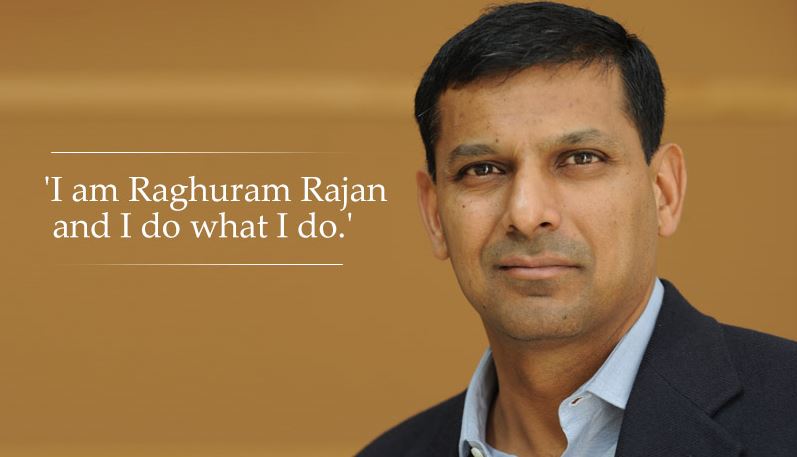सत्यदेव त्रिपाठी।
नासिरा शर्मा के साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उपन्यास ‘पारिजात’ का यह शीर्षक शब्द पीढ़ियों, संस्कारों, देशी-विदेशी संस्कृतियों और धर्मांे के द्वन्द्वों-तनावों व उपादेयताओं के साथ ही अतीत की स्मृतियों, वर्तमान की दमित इच्छाओं व अवशेष हसरतों तथा भविष्य के सपनों का वाहक-वाचक संकेत बनकर तो आया ही है, इन सभी रूपों का केन्द्रीभूत एक पात्र बनकर भी उपस्थित है- बल्कि यूं कहें कि इसका पात्रत्त्व प्रत्यक्ष रूप से अनुपस्थित होने के बावजूद पूरे में उपस्थित है- पूरी कथा और हर प्रमुख पात्र के मनों में ‘सबके दिल में है जगह तेरी’ बनकर। और इन सभी तरहों में अद्भुत रूप से साकार होता है ‘पारिजात’ का शीर्षकत्व और शीर्षक का पारिजातत्त्व- ‘पादपों में पारिजात’ जैसा।
पात्र के रूप में पारिजात है उपन्यास के नायक रोहन व उसकी ब्रिटिश प्रेमिका-पत्नी एलिस का दो साल का बेटा, जिसे लेकर गायब तो हो ही गई है एलिस, लेकिन रोहन पर बहुत सारे झूठे इल्जामात लगाके उसे जेल भी भिजवा चुकी है। और यह त्रासदी भी पूरे उपन्यास पर तारी है। पारिजात को पाने की तड़प व आतुर प्रतीक्षाओं में यूं अटकी हैं सबकी सदिच्छायें, कि गोया ‘हजार रंग से मुझको तेरी खबर आयी’ जैसी गुहार उपन्यास से आद्यंत आती रहती है। इतिहास के चरित्रों के मिस प्रतीकों में भी उमड़ता है दुख, पर उसमें टीपू सुल्तान, वाजिद अली शाह व बहादुर शाह जफर आते हैं- प्राण त्याग देने वाले हुमायूं नहीं और ‘राम राम कहि राम कहि, राउ गये सुरधाम’ वाले सर्वाधिक विश्रुत दशरथ तो कतई नहीं।
कथा व कृति का अंत रोहन की दूसरी शादी से होता है, तो उसकी मुस्लिम सास सोचती है- ‘मैं हर वह काम अंजाम दूंगी, जिससे पारिजात लौटे या परीजाद (के रूप में नया बेटा) आए’। इस तरह यह उपन्यास ‘पारिजात’ से ‘परीजाद’ तक की प्रतीक-कथा भी है। सास लेखिका भी है और आगे जोड़ देती है- ‘ताकि हमारे सूने घरों में बच्चे की किलकारी तो गूंजे’। रोहन की नयी पत्नी रूही भी अपनी मां की तरह मनाती है- मेरी बड़ी औलाद (पारिजात) जहां भी हो, उसे रोहन के सीने से लगा दे’ वरना ‘मेरा छोटा बेटा (भावी परीजाद) अपने बाप के सीने में सुलगती तपिश को ही हमेशा महसूस करेगा’… और इस तरह के ढेरों कथन हैं, अकूत व्यग्रताएं हैं, अनंत व्यथाएं हैं। रोहन खुद नेट पर इस कैफियत के साथ अपने पैत्तृक घर का पता डाल देता है, ताकि बड़ा होकर पारिजात कभी देखे, तो अपने दादा के घर आ सके। और पुत्र-पौत्र के मोह तथा कुल-खानदान की अनुरक्ति (आॅब्सेशन) यह सब इतना ज्यादा भी हो गया है कि कई बार तो पूरा उपन्यास इसी के लिए हो गया लगता है। इतनी गलदश्रु भावुकता भर उठी है, जो कई बार अउंजा (सफोकेट कर) देती है। फिर पंकज विष्ट आदि जैसे सोचू-विचारू लोग अब क्या कहेंगे, जो ‘मुझे चांद चाहिए’ की वर्षा के अपने भावी बेटे और उसके वारिस होने की दो पंक्तियों को बर्दाश्त न करके उसे दकियानूस और जाने क्या-क्या बनाने पर पिल पडेÞ थे। उनके चिंतकीय चश्मेबद से खुदा बचाये इस पारिजात-परिवार व उसकी जननी (स्रष्टा) को!
उपन्यास की नजरों से ओझल हुआ यह पारिजात अकेला वारिस है- तीन प्रगाढ़ मित्र परिवारों का। पहला है- रोहन के प्रोफेसर माता-पिता प्रभा व प्रह्लाद दत्त का परिवार। दूसरा परिवार नुसरत व बसारत का है, जिनका भी एक बेटा है- काजिम। तीसरा परिवार है- जुल्फिकार व फिरदौस जहां का, जिनके एक पुत्र मोनिस और एक लड़की रूही है। ये तीनों परिवार ‘हिन्दू-मुस्लिम एकता के द्वीप’ हैं और जब तीनों के बीच अकेली लड़की पैदा हुई- रूही, तो इनके उछाहोत्सव में बेटी-जन्मोत्सव की प्रगतिशीलता भी आ गयी, लेकिन फिर भी बेटा-विहीन परिवार नहीं रहा कोई। और चाहत तो दोनो पीढ़ियों (फिरदौस जहां व रूही) की पारिजात या परीजाद की ही रही- पारिजाता या परीजादी की नहीं।
सबके अंत में जन्मी यही मल्लिका-ए-जश्न रूही कथाकृति की नायिका है। तीनों परिवारों के चारों बच्चे भाई-बहनों की तरह साथ खेले और अपनी संस्कृति में पगे पिता-माताओं ने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा विदेश में ही दिलवायी- ‘हार्वर्ड में तीनों ‘थ्री कजिंस’ के नाम से जाने जाते थे’। चारों बच्चों में कुछ विनोदी-ठिठोली वाली दोस्ती काजिम-रूही-रोहन के बीच ही रही- मोनिस से तो हो नहीं सकती- एक दूध वाला सगा भाई जो ठहरा। लेकिन रूही की शादी भी रोहन से नहीं, काजिम से ही होती है। दूध का बराव भी और मुस्लिम का मुस्लिम भी- दोनों हाथ में लड्डू। बड़ा होकर भी रूही का भाई मोनिस विदेश में बसकर दरकिनार ही हो जाता है- अंदर वाले बाहरी नाते की ही तरह। लेकिन इधर काजिम के माता-पिता भी चल बसते हैं और एक्सीडेंट में कमर के नीचे शून्य हो गये अंगों की असहाय दयनीयता में काजिम भी आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से नुसरत-बसारत का पूरा परिवार पर्दे से तिरोहित हो जाता है।
उधर रूही के पिता भी चल बसते हैं। और अब इतने सारे दुखों की मारी विधवा रूही ही मायके में पांव से अशक्त मां व उनकी लालकोठी तथा ससुराल में खुद की व सफेद कोठी की संरक्षिका का दायित्त्व निभाती है। दोनो घर संभालने के इस मुकाम पर आकर पता चलता है कि काजिम व रूही की शादी की एक पेंच दोनों के लखनऊ स्थित इस कथा-ढांचे में भी है। उधर विदेशी पत्नी के जाल में फंसकर रोहन अपनी सारी पूंजी, इज्जत व बेटे को गंवा कर जेल की सजा काटता है। इसी चक्कर में मां-पिता की भी सारी कमाई फुंक उठती है। फिर इतने सारे गम में बेटे को छुड़ाने से लौटकर आयी रोहन की मां भी चल बसती हैं। और जब लुटा-पिटा रोहन लाचार होकर अपने देश और पिता के पास इलाहाबाद आता है, जहां से उपन्यास शुरू होता है, तो पिता के सपनों का महल (निजी बंगला) भी बिक चुका है। वे अपने पटु शिष्य निखिल व उसकी पत्नी शोभा, जो रोहन की मां की शिष्या भी रही है, के संरक्षण में रह रहे हैं। और इस रूप में नासिराजी एक और पुरानी परम्परा (गुरु-शिष्य) का भी निदर्शन करती हैं।
इस प्रकार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के पड़ोसी जिलों से निकलकर इलाहाबाद व लखनऊ में बस गए इन्हीं तीनों परिवारों की मूल कथा के कुल दस सदस्यों में अब पांच ही बचे हैं और विदेश-स्थित मोनिस (व उसके परिवार) को बाद कर दिया जाए, तो कथा चार सदस्यों में ही चलती है- रूही व उसकी मां तथा रोहन व उसके पिता। इसमें कथानायक रोहन के साथ हम इलाहाबाद से उसके गांव व फिर बचपन की हमराही सखी रूही के यहां लखनऊ तक की यात्रा करते रहते हैं, पर जो हाथ आना है, कि नायक को उसकी विदेशी पत्नी ने किस तरह और क्यों फंसा कर जेल करा दिया और संतान को ले उड़ी, वह छलता रहता है। समझ में आता है कथा के मूल को छिपाते हुए पाठक की उत्सुकता को बनाए रखने या बढ़ाने का लेखकीय गुर, पर उस मूल कथा के रहस्यों को सूचना की तरह जगह-जगह पर छींट-छिटका दिया जाना काफी कुछ को बिखरा भी देता है। अब लखनऊ में रूही-कथा का अध्याय चल रहा है, उसमें रोहन के पिता का अपनी स्वर्गीया पत्नी की डायरी पढ़ने का प्रसंग आ जाता है, जिसमें रोहन-एलेस की सनसनीखेज कथा का एक अंश चलने लगता है। ऐसी आवा-जाही बार-बार होती है, जिससे एक क्रमहीन संरचना-शैली बनती है, जो पाठकीयता को झटका देती रहती है।
यदि इसे पूरी संवेदना व शिद्दत के साथ एक जगह जमा कर कहना होता, तो उसका असर जबर्दस्त पड़ता। वह औपन्यासिकता का शृंगार बनता। लेकिन इस तरह से उत्सुकता तो बनती है, पर व्यतिक्रम की छाप उससे ज्यादा बनती है। कई बार तो औचित्य भी बाधित होता है। जैसे- रूही-रोहन का परिवार से लेकर निजी स्तर पर भी जितना गहरा घर जैसा सम्बन्ध है, उसे दिखाने में इतने सारे दृश्य, इतने छोटे-छोटे नैरेशन- जाने कितना फुटेज खा जाते हैं। पर एक तो कोई खास कलात्मकता नहीं बनती- सिवाय एक बार माफी मांगने के लिए रोहन का कबूतर लाके उड़ा देने वाले दृश्य के अलावा; और दूसरे इतने लम्बे अरसे तक दोनों के साथ रहने के बावजूद रोहन का राज खुलता नहीं। यह और असंगत तब हो जाता है, जब रूही अपना राज बता भी देती है कि उसके पति ने आत्महत्या की थी। वह हार्ट अटैक नहीं था, जैसा कि दुनिया में प्रचारित किया गया था। परंतु रोहन की त्रासदी न वह पूछती, न वह बताता। इसमें रोहन के मौन शोक का, उसके अंतर्मुख गम्भीर व्यक्तित्व का चाहे जितना प्रकटन हुआ हो, उन सम्बन्धों की अपूरणीय क्षति होती है, जिनकी गाथा गाते कृति थकती नहीं। और आखिर वह राज रूही के सामने उसकी विद्यालयीन सहपाठिनी मित्र मारिया के माध्यम से प्रकट होता है, जो केस के दौरान रोहन की काउंसिलिंग कर चुकी है। लेकिन उसके बाद का कथांत तो उपन्यासांत में ही जाकर आता है।
अब इस कथा-रचना को कुछ मासूम सवालों के बरक्स देखें, तो तीनों परिवारों पर थोक में आ पडेÞ दैहिक-दैविक-भौतिक तीनों तापों की आकस्मिकताएं पुन: चाहे जितनी औपन्यासिक हों, क्वचित-कदाचित जीवन में घटती भी हों, पर जीवन-यथार्थ से जुड़ी इस उपन्यास-विधा में ये सब लेखिका द्वारा की हुई ज्यादा, हुई कम लगती हैं- यानी घटित से ज्यादा नियोजित। कथा-नियोजन का इकतरफापन एलिस के अत्याचारों में भी है। हालांकि हवाला दिया गया है- ‘मध्य पूर्वी देशों में औरत की शिकायत पर कानून फौरन एलर्ट हो जाता है। एन्क्वायरी के बाद चाहे मर्द को मुजरिम न साबित कर पाए, पर बात औरत की सुनी जाती है’, फिर भी इतने पढ़े-लिखे व इतने बडेÞ अफसर रोहन के साथ ताबड़तोड़ इतना सबकुछ होते जाना भौतिक से अधिक दैवी प्रकोप या जादू-मंत्र जैसा लगता है। कृति में प्रत्यक्ष रूप से एलिस नहीं आती, पर उसका न आना अबोध शिशु पारिजात के न आने की तरह कलात्मक नहीं कहा जा सकता। वह एकमात्र विलेन है कृति की। रोहन के जरिये सबके भौतिक दुखों की कर्त्ता है- ‘सब अनरथ कर हेतू’। उसका पक्ष उसकी जानिब से भी आता, तो बात अधिक स्पष्ट व संतुलित होती। तब शायद और कुछ भी सामने आता। वरना नायक वाले अपने प्रिय पक्ष को विपक्ष के बयान से दूर रखना खटकता रहता है और उसके आने का खटका बना रहता है। बहरहाल, इससे अधिक मानीखेज सवाल है- कथा-विन्यास के तरीके का। सानुपातिक रूप से देखा जाए, तो यह जो त्रि-परिवार कथा है, वह कृति में अपेक्षाकृत कम स्थान पाती है। ज्यादा जगह घेरती है- धर्म व संस्कृति, शिया सम्प्रदाय में ताजिया, कर्बला-रामलीला आदि की बहु-बहुआयामी चर्चाओं से होते हुए हुसेनी ब्राह्मण वगैरह की बहुतेरी बातों के साथ परम्परा व इतिहास आदि भी, जिनमें समाया है लोक से लेकर ज्ञान-विज्ञान एवं कुरानशरीफ तक का बहुत-बहुत कुछ। निस्सन्देह यह सब बहुत महत्त्वपूर्ण है। आज जब वह सांस्कृतिक परिवेश लुप्तप्राय हो रहा है और इन चेतनताओं से वंचित नयी पीढ़ी ‘साक्षात् पशु: पुच्छविषाणहीन:’ की तरफ बढ़ रही है, नासिराजी का इन परिदृश्यों को सोद्देश्य रूप से भरपूर समाहित करना नितांत श्रेयस्कर है। किंतु ध्यातव्य है कि हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, जिस पर इनके वर्णन-विवेचन इस कदर हावी हो गए हैं कि जब चाहें, कथा पर अतिक्रमण कर देते हैं। एक उदाहरण दरपेश है- विदेश में अपना सब कुछ लुटाकर आया रोहन कितने तनावों में होगा, पर इसी में सफीर व अरशद हुसेन जैसे इतिहास-संस्कृति के प्रेमी पात्र आते हैं और बार-बार रोहन को ले जाते हैं पुरानी संस्कृति व धर्म की धरोहरों की खोजों-बहसों में। इसी तरह जब वह पुन: विदेश जाकर अपने को पुनर्नियोजित करने तथा खोए हुए को जितना कुछ बन पडेÞ, हासिल कर लेने की जद्दोजहद में लगा है, इन पात्रों के फोन आते हैं। रोहन कई बार बात भी करता है। इससे इन खोजी तत्त्वों के निदर्शन के साथ शायद नायक के चरित्र को उठाने की मंशा भी हो, पर उस मूड व उन हालात में यह सब कहीं ‘जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सोहात’ का सबब भी बनता है और स्वाभाविकता जाती रहती है।
इन ऐतिहासिक-सांस्कृतिक समावेशों के अलावा जुही की ससुराल व मायके वाले दोनों घरों के आधे दर्जन नौकर-नौकरानियां हैं, जो सोच के स्तर पर उदार व प्रगतिशील उन परिवारों के जीवन में रचे-बसे सामंती संस्कार को भी उजागर किए बिना नहीं रहते। और इनकी गतिविधियों के वर्णनों के साथ इनकी ढेरों कहानियां भी मुतवातिर चलती रहती हैं। माना कि यह सब नौकर-मालिक की डोर के अटूट लस्तगे हैं, पर ये भी उक्त चित्रणों की तरह अलग होकर छिटके रहते हैं। इनसे मूल कथा व पात्रत्त्व के साथ घर में होने के सिवा न कोई नाता बनता, न सरोकार, जिसके चलते इनके बिना कृति की कोई क्षति भी नहीं होती। हां, अन्ना बुआ बड़ी वफादार नौकर हैं, संतरा-मोसम्ही बड़ी नेक लड़कियां हैं, जो साबिर से बेपनाह प्यार करती हैं। जोहरा बी बड़ी राजदार सहेली हैं। यानी ये पारम्परिक घटकबद्ध पात्र हैं। और इन सब कुछ का इस कदर होना हुआ कि मूल कथा तो कई बार गोया इसी सबको गूंथने की अर्गला भर बन गई है- बल्कि रिक्त स्थान की पूर्त्ति (फिलर) भी कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी।
कुल मिलाकर मूल कथा से इतर या अवांतर वर्णनों का लम्बे कथांशों की तरह बारम्बार आते जाना ही इस कृति की शैली बन गई है, जिसमें कथा व इन विविध विषयों के वर्ण्य भी साफ-साफ दिखते हैं, पर दोनों ही अलग-थलग होने से बिखर जाते हैं और पाठक भटक उठता है- अनायास। कह सकते हैं कि उपन्यास कथात्मक से अधिक वर्णनात्मक हो गया है, क्योंकि वर्णनों की रौ में कथा भी कथात्मक कम ही रह पाती है। उसे वर्णनों-विवेचनों (नैरेटिव्स) में कथांश बन-बन कर घुसपैठिये की तरह बच-बचाके आना पड़ता है। यह सब नासिराजी के ‘ठीकरे की मंगनी’ व ‘कुइयांजान’ जैसी सुगठित रचनाओं से नितांत अलग हो गया है।
‘पारिजात’ से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि बड़ी फुर्सत में (भले समय निकालकर) लिखा गया है। लेखिका को कृति पूरा कर देने या अपनी बात को कह देने की कोई जल्दी नहीं है। और उसकी अपनी बात सचमुच वही है, जो कथा-इतर है। इससे गति की जगह ठहराव ही उपन्यास का स्थायी भाव बन गया है। ऐसे में रचना से ‘कालिदासो विलास:’ वाला कला-विधान अपेक्षित होता है- जैसा द्विवेदीजी के ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’, ‘पुनर्नवा’ और मनोहर श्याम जोशी के ‘कसप’ या सुरेन्द्र वर्मा के ‘काटना शमी का वृक्ष पद्मपंखुरी की धार से’ आदि में हुआ है। जिनमें कथा तो अल्प है, पर कृति में कथा से परे का पाठकीय सुख आने लगता है। लेकिन ‘पारिजात’ में वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता। विलास के बदले विस्तार, जिसे फैलाव भी कह सकते हैं, का भार सर पर जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, ‘साहित्य अकादमी’ से नवाजे जाकर बहुचर्चित होने और बड़ी जहीन व प्रतिबद्ध लेखिका की महत्त्वाकांक्षी रचना होने की सम्मान्य छाप वैसे ही वैसे घटने लगती है और उन सबसे बनी पने की अगाध उत्सुकता और भीनी-भीनी साध कम होती जाती है। हारकर हम पन्ने पलट-पलट कर कथा खोजने लगते हैं, जो मिल भी जाती है और मजा यह कि कथा और पाठकीयता को कोई नुक्सान भी नहीं उठाना होता।
इन नुक्सानों और उक्त कलात्मक हानियों के बावजूद विचारणीय यह भी है कि कथाकृति में संस्कृति, धर्म, इतिहास आदि की बातें कितनी आएं और कैसे? कथा या पात्र के जीवन का हिस्सा बनकर आने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कोई पात्र कर्बला में हिस्सा ले चुका होता या कोई हुसैनी ब्राह्मण अथवा उसके वारिस आदि होते, तब तो आंखों देखी व काया भोगी बातें आतीं। वे देश से विदेश तक फैले कथांचलों में कथा-चरित्रों से जुड़ते और वे बातें कथात्मक आसंग के साथ आतीं, तो औपन्यासिक कला का मामला बनता। पर यहां ऐसा किसी में भी नहीं होता, जिसके चलते दृढ़ता से लगने लगता है कि इन गम्भीर व शोधपरक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विषयों पर अलग से वैचारिक विधान की पुस्तक लिखी जाती, तो विषय के साथ न्याय होता, वरना हुसेनी ब्राह्मण जैसे जहीन विषय में दत्त लोगों के वहां जाने की स्थितियां और पहुंचने के हालात को इतिहास के बदले पौराणिक-साहित्यिक पात्र अश्वत्थामा और उनके छह साथियों से जोड़कर एक पैराग्राफ में साध दिया गया है। इस तरह कुछ भी करीने से नहीं आ पाता- न कथा, न कथेतर विवेचन। वे विवेचन औपन्यासिक विधान में अटक जाते हैं और उपन्यास उन इलाकों में भटक जाता है। फिर उपन्यास में उच्छिन्न की तरह आकर वह अपने सही पाठक तक पहुंचता भी नहीं।
उधर घोर नियतियों की शिकार कथा से समकालीन समय या चिरंतन विमर्श जैसा कोई खास कथ्य बनता नहीं और कथेतर समावेशों में ‘ईरान में कर्बला का पूरा वाकिया रामलीला की तरह खेला जाता है’ या दत्त लोग हुसेनी ब्राह्मण हैं- जैसे शोध या उद्भावना से निकले नतीजे किसी कारगर सरोकार (उपन्यास के गुण-धर्म) से जुड़ते नहीं। बात-बात में आई तमाम फुटकर टिप्पणियां अवश्य आज की विद्रूपता को खोलती हैं, पर स्फुट ही। जैसे- ‘डिग्री के आगे फन का कोई महत्त्व नहीं’, ‘पश्चिमी देशों के सेटअप एशियन देशों को एकाकी कर दे रहे हैं’, ‘पूरी कॉलोनी में जो भी बूढ़े हैं, उनके बच्चे या तो विदेशों में हैं या दूसरे शहरों में और वे या तो अल्लाह के भरोसे हैं या नौकरों के सहारे’।
इतने दैवी-दानवी झंझावातों से गुजरते नायक-नायिका में मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों का आना अस्वाभाविक न होता, पर सबको संतुलित रखते हुए ऐसे कुछ से साफ-साफ बचाकर उपन्यास भी ऐसी जटिल बारीकियों से बच निकलता है, किंतु रूही से रोहन की दूसरी शादी हुई देखकर प्रह्लाद दत्त के शिष्य निखिल की पत्नी शोभा की मित्र चन्द्रप्रभा का अचानक विस्फोट एक आक्रामक मनोवैज्ञानिक दृश्य खड़ा कर देता है। रोहन के प्रति उसके अनुराग का उद्गार पहले एक बार आया अवश्य था, पर तब मजाक में उसके मुंहफट स्वभाव का हिस्सा भर लगा था, जिसे बिना रचना में रसे-बसे इस तरह सबके सामने फट पड़ना न उसके प्यार की गहनता का परिचायक बन पाता, न किसी विरोध का। और फिर यह सब उपन्यास में अलक्ष्य होकर रह भी जाता है- लेखिका और चन्द्रमुखी दोनों ही तरफ से। कहना होगा कि जितने हल्के-फुल्के ढंग से पूरी कृति का विधान हुआ है, उतने ही सहज भाव से भाषा का भी वितान बना है। इसीलिए उसकी कोई विशिष्ट पहचान व प्रकृति सामने नहीं आती। बस, विषय के मुताबिक कहीं-कहीं उर्दू शब्दों की बहुतायत लक्ष्य की जा सकती है। और उसी तहजीब व तमद्दुन के कुछ तकनीकी शब्द भी मिलते हैं, जिनमें चन्द गिने-चुने शब्दों के अर्थ देखने भी पड़ते हैं। ‘बेवकूफ का दिल उसकी जुबान पर होता है और होशियार की जुबान उसके दिल में होती है’ जैसे अनुभव-सम्पन्न सूत्रात्मक वाक्य भाषा की छौंक के जीरे जैसा जायका देते रहते हैं।
और अंत में, ज्ञान-संस्कृति-इतिहास आदि की सारी कवायदों के बीच रोहन-रूही की शादी के कथा-निष्कर्ष को लेखिका जिज्ञासा बनाये रखने के लिए बचाती रही, पर कृति की हर शै उसका अनुमान देती रही, क्योंकि दोनों के सिवा और बचा ही कौन था? किंतु वह रूही की तरफ से जिस सीधे-सर्द व अनपेक्षित ढंग से आया कि उदास कर गया। फिर भी पिता का बिका बंगला वापस ले लिया गया, नायक-नायिका के टूटे जीवन जुड़ गये और पारिजात की चिंता से आकुल पूरा उपन्यास जिस शीघ्रता से परीजाद की कामना व पारिजात की वापसी की सदिच्छा वाले ‘की नोट’ के साथ पूरा हुआ, कि दादी मां की कहानियों के अंत ‘ऐसे ही सबके दिन फिरें’, की कामना लहलहा उठी।
पुस्तक- पारिजात (उपन्यास)
लेखिका- नासिरा शर्मा
प्रकाशक- किताब घर, नई दिल्ली
प्रकाशन- 2014