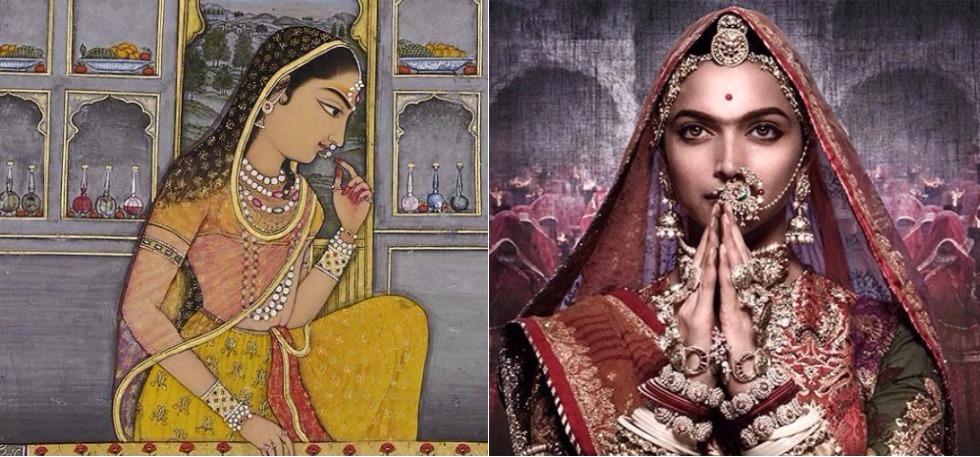प्रदीप सिंह (प्रधान संपादक/ ओपिनियन पोस्ट)
देश का संविधान बनने के बाद उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का गठन हुआ। इसके पहले सभापति बने तत्कालीन उप राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा की पहली बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सदन की सबसे बड़ी उपयोगिता यह होगी कि वह सुनिश्चित करेगा कि जल्दबाजी में कोई कानून पास न होने पाए। आज चौंसठ साल बाद राज्यसभा की स्थिति को देखकर डा. राधाकृष्णन क्या कहते इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। पर इतना विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वे खुश तो नहीं ही होते। भारत के संविधान का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जाहिर है कि द्विसदन (बाइकैमरल) व्यवस्था भी वहीं से ली गई। दुनिया के जिन भी देशों में द्विसदन की व्यवस्था है ज्यादातर ने उसे खत्म किया और कुछ समय बाद फिर बहाल किया। फर्क यह आया कि उच्च सदन के अधिकार कम कर दिए गए। भारत की संसदीय व्यवस्था परिवर्तन के उसी दौर से गुजर रही है। सवाल उठने लगा है कि क्या उच्च सदन निचले सदन से ज्यादा अहम है। निचले सदन यानी लोकसभा सीधे चुने हुए सदस्यों से बनती है। उसी सदन के बहुमत/अल्पमत से सरकारें बनती गिरती हैं। पिछले दो साल का अनुभव बताता है कि राज्यसभा की भूमिका के बारे में डा. राधाकृष्णन की जो मान्यता थी वह उससे काफी दूर निकल गई है। कानून इत्मीनान से बनाने की बजाय राज्यसभा कानून को बनने से रोकने का मंच बनती जा रही है। राज्यसभा लोकसभा से पारित किसी विधेयक पर और विचार विमर्श की जरूरत बताए यह तो समझ में आता है लेकिन विधेयक पेश ही न होने दे इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और अगर वह लोकसभा चुनाव में हार के बदले का मंच बन जाए तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। इस समय यही हो रहा है। इस स्थिति में किसी बदलाव के लिए भी जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सवार्नुमति बने। निकट भविष्य में तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती।
राज्यसभा का यही एक संकट नहीं है। दूसरा संकट भी कम गंभीर नहीं है। बल्कि यह तय करना कठिन है कि कौन सा ज्यादा गंभीर है। राज्यसभा की कल्पना एक ऐसे सदन के रूप में भी की गई थी जिसमें प्रबुद्ध और विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों को सदस्य बनाने में वरीयता दी जाएगी। ऐसे सदस्य लोकसभा के विधायी कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा सकेंगे। उन पर किसी मसले पर अपनी राय कायम करते समय इस बात का दबाव नहीं होगा कि ऐसी राय देने के कारण चुनाव तो नहीं हार जाएंगे। पर क्या डा. राधाकृष्णन और संविधान निर्माताओं ने इस बात की कल्पना भी की होगी कि विधायकों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर कोई भी उच्च सदन का सदस्य बन सकेगा। क्या इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पार्टी नेतृत्व का कृपापात्र और धनबल ही आधार बन जाएगा। जिस व्यक्ति को उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच के आधार पर राज्यपाल विधान परिषद में नामजद करने से इनकार कर दें, क्या उसे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए। कैमरे पर विधायकों को वोट के बदले रिश्वत देने का प्रस्ताव करने वाला राज्यसभा का सदस्य बनेगा और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा तो उच्च सदन की गरिमा का क्या होगा। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए विधायकों के वोट दो तरह से बिक रहे हैं। पहला तरीका विधायकों की फुटकर खरीद का है। दूसरा तरीका पार्टियों से थोक में उनके विधायकों को खरीदने का है। पार्टियां इसके लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अपने अतिरिक्त वोट के आधार पर किसी पैसे वाले को चुनाव में उतारने या समर्थन देने का और क्या कारण हो सकता है। विधायक फुटकर में बिके तो बिकने और खरीदने वाले दोनों फंस सकते हैं। जैसा कुछ साल पहले झारखंड में हुआ। लेकिन पार्टियां वोट बेचें तो किसी को कोई एतराज नहीं। यह सिलसिला नया नहीं है। इतना जरूर है कि यह दिन पर दिन गंदा होता जा रहा है। इस मामले में राजनीतिक दलों में अब आंख की शर्म भी नहीं बची है।
राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के ताजा दौर ने एक बार फिर उच्च सदन की सदस्यता पाने के तरीकों को राष्ट्रीय विमर्श में ला दिया है। समस्या इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि मौजूदा व्यवस्था में सबका निहित स्वार्थ है। चुनाव में पैसे की भूमिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव ही नहीं पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव भी पैसे का खेल बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा टिकट मिलने की गारंटी बन जाता है और चुनाव में जीत की संभावना बढ़ा देता है। पार्टी के लिए जीवन लगाने वाले कार्यकर्ता का टिकट जब कोई थैलीशाह काट देता है तो उसे समझ में नहीं आता कि किससे फरियाद करे। यकीन न हो तो कर्नाटक के दानिश अली से पूछिए। उनके साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है। यह माहौल बना रहा तो राजनीतिक दलों को समर्पित कार्यकर्ता कहां से और क्यों मिलेंगे।