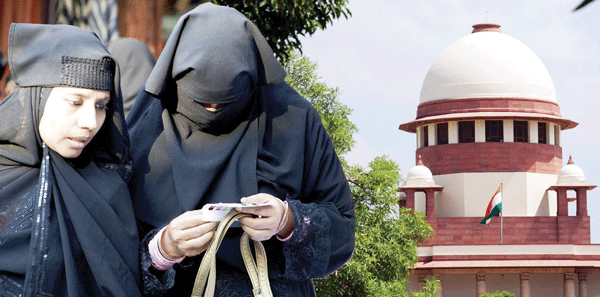जिरह/प्रदीप सिंह
लेखक और फिल्मकार गुलजार साहब का कहना है कि लेखक समाज के जमीर का रखवाला होता है। सैद्धांतिक रूप से तो उनकी बात सही है। लेकिन क्या अपने देश में आज ऐसी स्थिति है। इस सवाल का जवाब हां में देना सचाई से मुंह मोड़ने जैसा होगा। आज की बात इसलिए कि एक समय था जब लेखक समाज की अतंरात्मा का वास्तव में रखवाला था। हिंदी लेखकों की बात करें तो जब मुंशी प्रेम चंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, जैसे बहुत से लेखक थे जिनकी रचनाएं पाठक खोजकर और खरीदकर पढ़ता था। आज कितने लेखक हैं जिनकी किताबें खरीद कर पढ़ी जाती हैं। पुस्तकों की सरकारी खरीद पर जीवित लेखक क्या समाज के जमीर के रखवाले हो सकते हैं। अगर ये होते तो लोगों तक इनकी बात जरूर पहुंचती। आज के ज्यादातर लेखक समाज से कटे हुए हैं, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं समाज के जमीर के रखवाले चयनात्मक कैसे हो सकते हैं। उनका जमीर कुछ खास मौकों पर ही क्यों जागता है। या यह भी कह सकते हैं कि कुछ खास मौकों पर खामोश क्यों रहता है। रखवाला तो हर समय सजग रहता है। यह चयनात्मकता ही उनके सरोकार को संदिग्ध बना देती है। कश्मीर के पत्रकार और साहित्यकार गुलाम नबी खयाल के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी के दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार लिया था और आज लौटा रहे हैं। इमरजेंसी में उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई खतरा नजर नहीं आया, आज आ रहा है।
अशोश वाजपेयी लेखकों के विरोध के अगुआ बन कर उभरे हैं। वे कलबुर्गी, पनसरे और दाभोलकर की हत्या से विचलित हैं। उन्हें दादरी कांड में मोहम्मद अखलाक की मौत का भी दुख है। उन्हें लगता है कि देश में सहिष्णुता खतरे में है और अभिव्यक्ति की आजादी संकट में। खासतौर से केंद्र में नरेन्द्र मोदी ( किसी ने सीधे मोदी का नाम नहीं लिया है) के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद। उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल से लेकर तमाम साहित्यकारों लेखको ने कमोबेश ऐसी ही बातें कही हैं। ये वही अशोक वाजपेयी हैं जिन्होंने भोपाल गैस कांड में सैकड़ों लोगों के मरने के बाद विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जब पूरा भोपाल शहर उस समय मौत और दर्द मंजर नजर आ रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के भोपाल ब्यूरो प्रमुख एनके सिंह ने जब इस आयोजन के समय पर उनसे सवाल पूछा था तो उनका जवाब था कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। अशोक वाजपेयी की राजनीतिक निष्ठा के बारे में भी कोई संदेह नहीं है। उन्हें दुख तो इस बात का भी है कि नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी और निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा जाता तो कहने वाले को फासीवादी और जनतंत्र विरोधी घोषित कर दिया जाता।
साहित्य अकादमी देश की करीब चौबीस भाषाओं में हर साल करीब इतने ही पुरस्कार देती है। अकादमी की स्थापना मार्च 1954 में हुई थी। करीब चालीस लेखकों ने अकादमी पुरस्कार लौटाए। इनमें मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती भी हैं। कृष्णा सोबती ने किसी सरकार से कभी कोई पद नहीं लिया और न ही पद्म पुरस्कार। इन चालीस में से कितने हैं जो उनके रास्ते पर चले या चलने की हिम्म्त रखते हैं। दरअसल अकादमी पुरस्कार लौटाने वालों में ज्यादातर अकादमी के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर निशाना साध रहे थे। उन्हें दो आपत्तियां थीं। एक कर्नाटक में कलबुर्गी के मरने पर साहित्य अकादमी ने कोई आधिकारिक शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया। दूसरे प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। खासतौर से मोहम्मद अखलाक की हत्या पर। दोनों आपत्तियां जायज लगती हैं। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री से मिलने या बात करने की कोई कोशिश नहीं की। बुद्धिजीवियों की प्रधानमंत्री से सीधी अपील थी कि वे देश में बढ़ रहे असहिष्णुता के माहौल पर कुछ बोलें। वे बोले पर इससे बुद्धिजीवीयों का अंसतोष कम नहीं हुआ। वे प्रधानमंत्री से सशर्त उदारता चाहते हैं। शर्त यह कि उदारता का प्रमाण देने के लिए वे वही बोलें जो बुद्धिजीवी चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन से बोले। तो उसे नाकाफी और देर से बोलना माना गया।
किसी पक्ष में खड़े लोगों की वाजिब बात भी अपना असर खो देती है। कोई मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति मोहम्मद अखलाक की हत्या का समर्थन नहीं कर सकता। दादरी घटना के विरोध में जब लेखकों/ बुद्धिजीवियों की आवाज उठती है तो आम आदमी के मन में कई सवाल उठते हैं। उसे लगता है कि जब कश्मीर से चुन चुन कर लाखों हिंदुओं को निकाल दिया गया या मार दिया गया तो ये लोग कहां थे। जब देश की राजधानी में दिन दहाड़े सीढ़े तीन हजार सिखों का मारा-जलाया गया तो इनकी जबान खामोश क्यों थी? इसलिए ये लोगो समाज की अंतरात्मा के रखवाले नहीं कुछ राजनीतिक ताकतों के हितों के रखवाले हैं। यही वजह है कि इनका विरोध जितना मुखर होता है, आम लोगों पर उसका असर उतना ही कम।